जनविरोधी हैं नए आपराधिक न्याय कानून
केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों और कठोर कानूनों को पेश करने को इस आधार पर सही ठहराने के लिए अभिनव लेकिन कुटिल प्रयास किए हैं कि मौजूदा कानून 'औपनिवेशिक' था और जो बदला जा रहा था वह भारत विरोधी था
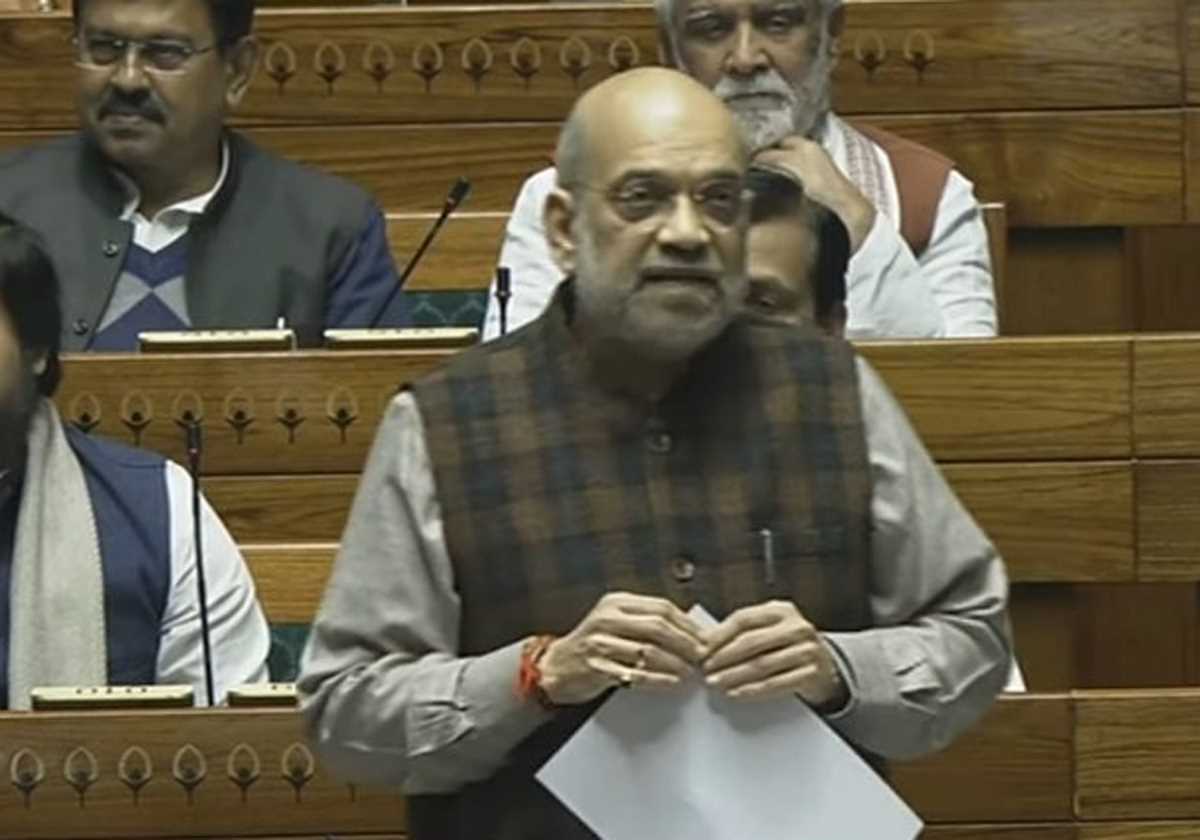
- डॉ.कॉलिन गोंजाल्विस
आपराधिक न्यायशास्त्र के दायरे के मद्देनजर यह मान लेना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून जन-विरोधी और मानवाधिकार विरोधी थे, शायद एक गलती होगी। अंग्रेजों ने आपराधिक कानून के कुछ सिद्धांतों को विकसित किया जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद द्वारा कई मौजूदा आपराधिक कानून विधियों को अपनाया गया था।
केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों और कठोर कानूनों को पेश करने को इस आधार पर सही ठहराने के लिए अभिनव लेकिन कुटिल प्रयास किए हैं कि मौजूदा कानून 'औपनिवेशिक' था और जो बदला जा रहा था वह भारत विरोधी था, लेकिन पुराने कानून के साथ तुलना करने से पता चलता है कि नए कानून प्रतिगामी हैं और स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश कानून की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं।
नए कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन्हें संसद ने विपक्ष के 140 सांसदों की अनुपस्थिति में पारित किया है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र के दायरे के मद्देनजर यह मान लेना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून जन-विरोधी और मानवाधिकार विरोधी थे, शायद एक गलती होगी।
अंग्रेजों ने आपराधिक कानून के कुछ सिद्धांतों को विकसित किया जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद द्वारा कई मौजूदा आपराधिक कानून विधियों को अपनाया गया था। वास्तव में ब्रिटिश काल से आधुनिक भारत तक समय के साथ आपराधिक कानून संरक्षण कैसे बिगड़ गया, इस बात का अध्ययन यह बताएगा कि भारत में आज कानून बनाने की प्रक्रिया ने बहुत दमनकारी ढांचे की ओर एक तेज मोड़ लिया है जो पहले से मौजूद स्वतंत्रता को कुचलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीन नए अधिनियमित कानून इसके उदाहरण हैं। आपराधिक कानून सिर्फ एक क़ानून के शब्द नहीं हैं बल्कि न्यायिक व्याख्या के साथ प्रभावित शब्द हैं। जब उन कानूनों को यांत्रिक और आकस्मिक रूप से बदला जाता है तो न्यायशास्त्र के सभी व्यापक निकाय कानून के साथ गायब हो जाते हैं।
तब कानून को बदलने के लिए कानून निर्माता के अनियमित निर्णय से कानूनी लड़ाई का इतिहास दूर हो जाता है। अंत में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, कानून में इस आकस्मिक परिवर्तन के लिए एक और भयावह अंतर्निहित कारण है- वह है अतीत में जो अच्छा है उसे नष्ट करना और वर्तमान को भ्रमित करना। जो बात समझ में आती है, वह है भारत में मानवाधिकार संरक्षण के ताने-बाने को नष्ट करने और भारत के लोगों पर नियंत्रण करने तथा दमन करने के लिए केंद्र की शक्ति को बढ़ाने की केंद्र सरकार की मंशा।
आईपीसी की धारा 124ए में राजद्रोह कानून को ही ले लीजिए जो इन शब्दों से शुरू होता है- 'शब्दों से कोई भी...' राजद्रोह ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दंडित किया है। इसे असहमति, विशेष रूप से अहिंसक असंतोष को अपराध (घोषित करने) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत क्राउन के खिलाफ प्रयुक्त किए गए कड़े शब्द अपने आप में राजद्रोह के आरोप और जेल में लंबे समय तक सजा के लिए पर्याप्त थे। 1968 में इसमें बदलाव की उम्मीद थी जब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने केदारनाथ के मामले में अपना फैसला सुनाया एवं प्रिवी काउंसिल से असहमति जताते हुए कहा कि चाहे कितने भी कड़े शब्द कहे गए हों- बिना किसी हिंसा के केवल शब्द राजद्रोह के आरोप में नहीं आएंगे।
इस आरोप पर अमल करने के लिए राज्य के खिलाफ विद्रोह के साथ-साथ हिंसा के लिए उकसाने वाले शब्द भी जरूरी थे। इस फैसले के बावजूद पत्रकारों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर सैकड़ों मुकदमे जारी रहे। यही कारण है कि एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के सभी मुकदमों पर रोक लगा दी। ...तो, यह सरकार क्या करती है? इस सरकार ने राजद्रोह शब्द के उपयोग को हटा दिया है। इसके बाद यह पुरानी धारा (राज्य के खिलाफ अपराध, धारा 152) को फिर से परिभाषित करता है, शुरुआत को बरकरार रखता है और शब्दों के साथ शुरू होता है, 'जो भी ... शब्दों से...' इस प्रकार, भले ही हिंसक कृत्यों का पालन न किया जाए, केवल शब्द ही अपराध के लिए पर्याप्त होंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में दी गई एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा है। जाति आधारित आरक्षण के विरोध में बनी फिल्म ' ओरे ओरु ग्रामाथिले' पर प्रतिबंध लगाने के मामले में 1989 में एस. रंगराजन बनाम जगजीवन राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'प्रदर्शन और जुलूस की धमकी या हिंसा की धमकियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता।'
पीठ ने अपने फैसले में लिखा कि 'राज्य खुली चर्चा और खुली अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकता है भले ही यह उसकी (राज्य की) नीतियों के लिए द्वेषपूर्ण हो।' अदालत के अनुसार सार्वजनिक हित के लिए वास्तविक खतरा 'फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग से नहीं बल्कि राज्य द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न होता है।' इसलिए नए कानूनों का सबसे क्रूर हिस्सा भाषण और असहमति का गला घोंटना है। ब्रिटिश कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 15 दिन थी। यह हिरासत पुलिस हवालात में होती है जहां कि यातना दी जाती है। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी समझा कि अगर यातना को कम करना है तो पुलिस हिरासत को कम से कम रखा जाना चाहिए। अब सरकार ने पुलिस हिरासत को 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी कानून पेश करने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में ऐसा भयानक प्रावधान नहीं है। यह समझते हुए कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद की अवधि का उपयोग पुलिस द्वारा यातना देने के लिए किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु मामले (1996 के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल) में गिरफ्तारी या हिरासत के मामलों में पालन की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताओं को निर्धारित किया।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी होने पर पुलिस को गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना था, गिरफ्तारी का स्थान और समय बताना था और इस मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, कई दिनों तक यातना देना और फिर आरोपी को बाद में गिरफ्तार दिखाया जाना आम बात थी ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर लगी कोई भी चोट गिरफ्तारी से पहले लगी हुई दिखाई दे। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटे में एक सार्वजनिक अस्पताल में जांच की जानी थी और एक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया गया था। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को एफआईआर के साथ गिरफ्तारी का ज्ञापन और मेडिकल रिकॉर्ड भेजा जाना था। अदालत के दिशा-निर्देशों को हर पुलिस स्टेशन में प्रदर्शित किया जाना था। नए कानूनों में इन दिशा-निर्देशों का पता नहीं है। इसलिए नए कानून यातना को बढ़ावा देने वाले कानून हैं।
जनता की शिकायतों को स्वीकार नहीं करने और विशेष रूप से शक्तिशाली लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने की पुलिस की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी मामले (ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2013) में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी तत्काल दर्ज की जानी चाहिए और इस बहाने को खारिज कर दिया कि चूंकि पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही थी इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। नए कानून में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत प्रारंभिक जांच कराने को सामान्य नियम बना दिया है। अंत में, आतंकवाद के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में प्रावधान को सामान्य आपराधिक कानून में प्रत्यारोपित किया गया है। आश्चर्य इस बात पर होता है कि यह दोहराव क्यों है।
इसका कारण खोजना मुश्किल नहीं है। सार्वभौमिक रूप से आतंकवाद कानून के क्रूर रूप में निंदा की गई थी जिसमें दो सुरक्षा उपाय थे जो जांच अधिकारी की शक्तियों को कम करते थे। सबसे पहले, जांच अधिकारी को सबूत इक_ा करने के बाद सरकार से मंजूरी लेनी थी और इसके अभाव में अभियोजन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था। दूसरे, एकत्र किए गए सबूतों का आकलन करने और आतंकवाद के लिए अभियोजन को आगे बढ़ाने के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को 'प्राधिकरण' के रूप में नियुक्त किया गया था। जब तक इन दोनों सुरक्षा उपायों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता तब तक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता था। तैयार किए गए नए कानूनों में ये दोनों सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं। नतीजतन, अब दो सुरक्षा उपायों के बिना यह एक नया गंभीर क़ानून है जो इसे दोगुना कठोर बनाता है।
(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)


